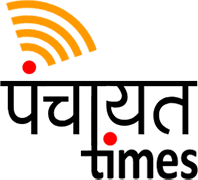नई दिल्ली. 17 नवंबर को 16वें वित्त आयोग (Finance Commission) ने अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी। अब इस रिपोर्ट को लेकर कई महत्वपूर्ण उम्मीदें हैं।
क्या हैं मुख्य अपेक्षाएं?
सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि आने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्र सरकार के राजस्व पूल से राज्यों को मिलने वाले हिस्से (vertical devolution) का प्रतिशत तय किया जाए। इसके साथ ही राज्यों के बीच इस हिस्से का वितरण कैसे होगा (horizontal distribution)यह भी रिपोर्ट में स्पष्ट होना चाहिए। यह सब संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत अनिवार्य है।
पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के लिए क्या अपेक्षाएं हैं?
दूसरी अहम उम्मीद यह है कि वित्त आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए ठोस सुझाव दे, जैसा कि अनुच्छेद 280(3)(bb) और (c) में कहा गया है। भारत की तरह कई संघीय ढांचों में स्थानीय निकाय ही पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण सड़कें और सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके लिए उन्हें संपत्ति कर, विज्ञापन कर और अन्य गैर-कर राजस्व जैसे बाजार शुल्क, टोल आदि वसूलने का अधिकार है। लेकिन राजस्व और खर्च की जिम्मेदारियों के बीच भारी अंतर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाता है।
क्यों है राज्यों के बीच इतना अंतर?
73वें और 74वें संविधान संशोधनों के तहत, राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे पंचायतों और नगरपालिकाओं को कौन-सी वित्तीय शक्तियाँ और कौन-सी जिम्मेदारियां सौंपेंगे। इसी कारण अलग-अलग राज्यों में स्थानीय निकायों की शक्तियां बहुत भिन्न हैं।
आदर्श स्थिति में, स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां और उनकी वित्तीय शक्तियां एक दूसरे से मेल खानी चाहिएं, पर ऐसा नहीं है।
11वीं और 12वीं अनुसूचियों में पंचायतों के लिए 29 और नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय सूचीबद्ध हैं, लेकिन ये अनुशंसात्मक हैं, बाध्यकारी नहीं। केंद्र और राज्य सरकारें आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय से जुड़े योजनाएं बनाती हैं और उनका क्रियान्वयन स्थानीय निकायों के जिम्मे आता है। अक्सर राज्य सरकारें स्थानीय निकायों पर नई जिम्मेदारियाँ तो डाल देती हैं लेकिन न उनके लिए राजस्व का प्रबंध करती हैं और न पर्याप्त कर्मचारी देती हैं। इसका असर पंचायतों और नगरपालिकाओं की विकास योजनाओं और रोजमर्रा की कार्यक्षमता पर पड़ता है।
राज्य वित्त आयोग (SFC) की भूमिका क्या है?
हर पांच साल में राज्य अपनी स्टेट फाइनेंस कमीशन (SFC) बनाते हैं। यह आयोग राज्य विधानमंडल को सुझाव देता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं को राज्य के राजस्व में हिस्सा मिले, उन्हें नए राजस्व स्रोत दिए जाएं,उन्हें अनुदान (conditional और unconditional) मिले, उन्हें और प्रशासनिक अधिकार व अधिकारी दिए जाएं। अब तक सौ से अधिक SFC रिपोर्टें पेश की जा चुकी हैं, लेकिन बहुत कम राज्यों ने वास्तव में उन्हें लागू किया। ऐसी स्थिति में स्थानीय निकाय केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता पर ही निर्भर रह जाते हैं। यही कारण है कि संविधान के तहत यूनियन फाइनेंस कमीशन (UFC) को स्थानीय निकायों के लिए राज्यों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने वाले सुझाव देने होते हैं।
पिछले यूनियन फाइनेंस कमीशनों ने क्या किया?
अब तक छह UFC की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं, लेकिन वे भी स्थानीय निकायों की वास्तविक वित्तीय जरूरतों का आकलन नहीं कर सके और केवल लंपसम (एकमुश्त) अनुदान देने की व्यवस्था की।
13वें UFC ने पहली बार सुझाव दिया कि स्थानीय निकायों को केंद्र के कर-योग्य राजस्व (divisible pool) में एक निश्चित प्रतिशत मिले।
इसके दो फायदे थे —
महंगाई का असर कम होता,
केंद्र के बढ़ते राजस्व का लाभ स्थानीय निकायों को भी मिलता।
लेकिन अगली UFC ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया और फिर से लंपसम अनुदानों की तरफ लौट आई। 15वें UFC ने भी यही तरीका अपनाया।
शर्तों (performance grants) में भी असंगतियां
13वें, 14वें और 15वें UFC ने अनुदानों को दो हिस्सों में बांटा —
बेसिक ग्रांट (बिना शर्त)
परफॉर्मेंस ग्रांट (कुछ शर्तों के आधार पर)
पर हर बार शर्तें नई थीं।
13वीं UFC ने छह शर्तें रखीं, जिन्हें ज़्यादातर राज्य पूरा ही नहीं कर पाए।
14वीं UFC ने उन शर्तों को खारिज किया और नई शर्तें दे दीं।
15वीं UFC ने फिर पूरी तरह अलग शर्तें पेश कर दीं।
यानी तीनों आयोगों में निरंतरता नहीं थी।
16वें वित्त आयोग से क्या उम्मीद है?
उम्मीद है कि 16वां UFC इन पुरानी समस्याओं से आगे जाकर 2.7 लाख पंचायतों और लगभग 5,000 नगरपालिकाओं की वास्तविक संसाधन आवश्यकताओं का आकलन करेगा, ताकि ये संस्थाएँ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के असली स्तंभ बन सकें।