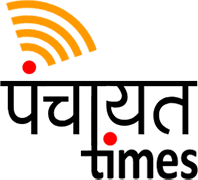नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए साफ किया है कि संसद या राज्य विधानमंडल (Legislature) द्वारा बनाया गया कोई भी कानून Contempt of Court (अवमानना) की श्रेणी में नहीं आता, जब तक वह संविधान (Constitution) के खिलाफ घोषित न किया गया हो।
जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह फैसला समाजशास्त्री नंदिनी सुंदर की 2012 में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। यह याचिका छत्तीसगढ़ में Salwa Judum, SPOs (Special Police Officers) और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लेकर थी।
क्या था मामला? | Chhattisgarh SPO Act और कोर्ट का निर्देश
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जुलाई 2011 के आदेश के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force Act, 2011 पारित कर दिया, जिससे पुराने SPOs को वैधता दे दी गई। याचिका में कहा गया कि यह कानून सीधे तौर पर कोर्ट के आदेश की अवमानना है क्योंकि कोर्ट ने SPOs के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी।
इसके साथ ही आरोप लगाए गए कि Salwa Judum के पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया , सुरक्षा बलों ने स्कूलों और आश्रमों से कब्जा नहीं हटाया और SPOs को निरस्त्र करने के बजाय उन्हें नए कानून से “वैध” कर दिया गया
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि यह अवमानना नहीं?
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी न्यायालय के आदेश के बाद भी यदि संसद या विधानमंडल कोई नया कानून पारित करता है, तो उसे केवल इस आधार पर अवमानना नहीं माना जा सकता। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संवैधानिक संतुलन जरूरी है। कोई भी कानून तब तक वैध रहेगा जब तक कि उसे संवैधानिक न्यायालय असंवैधानिक घोषित न कर दे।कोर्ट ने कहा, “यदि कोई पक्ष उस कानून को रद्द कराना चाहता है, तो उसे संबंधित कोर्ट में संवैधानिक चुनौती के रूप में ले जाना होगा, न कि अवमानना याचिका के रूप में।”
अदालत की दृष्टि से संवैधानिक संतुलन क्यों ज़रूरी?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में Rule of Law और separation of powers का पालन जरूरी है।Legislature को कानून बनाने की पूरी स्वतंत्रता है, बशर्ते वह संविधान के अनुरूप हो।न्यायपालिका का कार्य किसी कानून की संवैधानिकता जांचना है, न कि उसे उसकी विधायी प्रक्रिया पर रोक लगाना।